‘हिंदी का विवरणात्मक व्याकरण’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Hindi Grammar’ using the download button.
हिंदी का विवरणात्मक व्याकरण – Hindi Grammar PDF Free Download
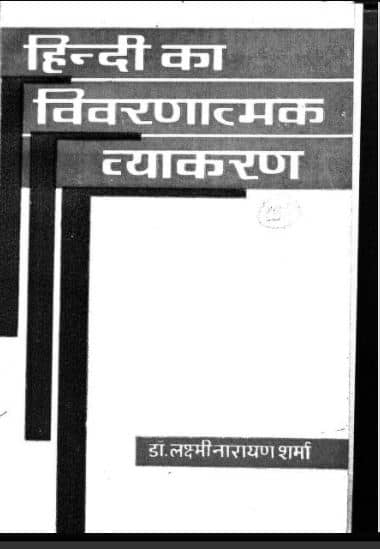
हिंदी का विवरणात्मक व्याकरण
बावश्यकताओों सया कथन-कैलियों के भाषाों के शब्दों, प्रश्नों, कहावतों, मुहावरे, अर्थों में (लिपि-चिह्नों में भी) परिवर्तन होता रहता है, किन्सु यह परिवर्तन बहुत ही धीरे-धीरे होता है ।
इस परिवर्तन को हम एक ही जन्म में प्रावः आसानी से नहीं पकड़ पाते । एक ही समय के पहले- लिखे और बाद लोगों की भाषा में चोड़ा-बहुत अन्तर हुआ ही करता है।
विज्ञान, कार्यालय, विधि, रेडियो समाचार, विज्ञापन,अध्यापन की भाषा में जो अंतर देखने में बाता है, उसे सैली-भेद या प्रयुक्ति वेद कहा जाता है।
हिन्दी की दो प्रमुख शैलियाँ प्रचलित है-1. साहित्यिक बैली 2. बोलचाल की शैली। अंग्रेजी, न्यू के प्रभाव से दो और पीलिया प्रचलित हो पनी है
भाषा कभी भी सीली-सुनत नहीं हो पाती, अतः व्याकरण में भाषा-विश्लेषण के समय मै तो-नेट से आए भाा परिवर्तन को नकारा नही जा सकता ।
व्याकरण-भाषा के फलों तथा प्रयोगों में तमानता, स्मृता तथा मानकता जाने के लिए और उन का ठीक- छींक विसलेसन- वित्तेन करने के लिए कुछ नियमों का होना मन कार्य है ।
व्याकरण इन्हीं नियमों का निरयग करनेवाला पास्तर है । अभिव्यक्ति-स्तर पर भाषा के दो मुख्य रूप (रचित, लिखित) होते हैं । भाषा का कथित रूप नय म और शक्ति का नाँ से बनता है ।
इन्टी स्यनियों और वनों से बाह्य, पय, पदबंध, उपवाक्य और वाक बनाते हैं । शम्दो पदीं, यदवन्धों और वाक्यों में गुस्सा और प्रयोगों के नियमों का बोध वारानेवाला शास्त्र व्याकरण (वि+आ+ करण वी भौति [समझाना ) कहते है
व्याकरण के नियमों से अनुशासित रहने पर भाषा के क्यों और प्रयोगों में स्थिरता, समानता तथा शुद्धता बनी रहती है किंतु कुछ शताब्दियों के बाद भाषा के प्रिवर्तित रूप के अनुसार व्याकरण के नियम |
वाक्योच्चारण के समय घोष तथा अधघोष ध्वनियों का प्रयोग होता है। घोष ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वरतन्त्रियों में होनेवाली’ कम्पन-आवृत्ति (#760प०7९५ ग शात्रब्ांणा) सुर (०7) या तान (7076) कहलाती है ।
एकाधिक घोष ध्वनियाँ लगातार उच्चरित होने पर सुर-लहर/अनुतान का निर्माण करती हैं, यथा—मैं अभी नहीं जाऊंगा वाक्य-उच्चारण के समय म्, ऐं, अ, भू, ई, नू, अ, हू, ईं, जू, आ, ऊँ, गूृ, आ’ 4 भिन्न-भिन्न सुर परस्पर मिल कर एक विशेष प्रकार की सुर-लहर का निर्माण करते हैं ।
अधघोष ध्वनियों के उच्चारण के समय अत्यल्प कम्पन होने के. कारण सुर का अभाव रहता है ।
वाकयों में अघोष ध्वनियों (लगभग 20%–229) .. की अपेक्षा घोष ध्वनियों (लगभग 78% –80%) का व्यवहार अधिक होने के
कारण वाक्यों में आदूयन्त सुर लहर/अनुतान की’ प्रतोति होती’ हैं। अतः वाक्यचारण के समय ध्वनियों के सुरों के आरोहावरोह का क्रम अनुतान कहलाता है ।
लगभग सभी भाषाओं में अनुतान-भिन्तता से वाक्य /वाक््यांश में अथ-भिन्नता आ जाती है, यथा– वे आ गए ।
” वाक्य को तीन प्रकार की अनुतान में बोलने पर तीन प्रकार के अथ की सूचना मिलती है–सामान्य कथन, प्रश्सूचक कथन आश्चयंसूचक कथन ।
हिन्दी को अच्छा’ शब्द विभिन्न अनुतानों में बोलने पर विविध प्रकार के अर्थों का सूचक होता है, यथा–द तुम्हारा यह नौकर तो अच्छा लगता है (>भला) । हरीश भी पास हो गया अच्छा ! (>-आश्चय) ।
बहुत देर से लिख रहे हो, अब लिखना बन्द करो; अच्छा (>> अनिच्छा) । हमें अभी चल देना चाहिए; अच्छा । (स्वीकृति)। आप इस बात का अर्थं समझ रहे हैं न ? अच्छा | (जी हाँ) ह हिन्दी में सामान्यतः तीन प्रकार के अनुतान-साँचे मिलते हं—. निम्त 2. सामान्य 3. उच्च। कभी-कभी अति उच्च या अत्यन्त उच्च अनुतान-साँचा भी मिल जाता है । निम्त को अवरोही (४2078) “|,
सामान्य को सम और उच्च को आरोही (7४78) ,/7 भी कहा जाता है। आरोह-अबरोह के मिश्चवित रूप को आरोहावरोह (एरंशा।8 40798) //”; अवरोह-आरोह के मिश्रित _ रूप को अवरोहावरोह (थि8-7878) ५ कहते हैं। .
आछ हिन्दी में सामान्यतः पाँच प्रकार के वाक्यों (सामान्य, प्रश्ससूचक, आश्चय॑. सूचक, आज्ञासूचक, निर्षेधसूचक) और अभिवादन के लिए कई प्रकार के अनुतान-साँचों का प्रयोग होता है, यथा–. सामान्य (निश्चयाथेक) वाक्यों में 2 3 । के अनुतान-साँचें का प्रयोग होता
| लेखक | लक्ष्मीनारायण शर्मा – Lakshminarayan Sharma |
| भाषा | हिन्दी |
| कुल पृष्ठ | 616 |
| Pdf साइज़ | 174 MB |
| Category | विषय(Subject) |
हिंदी का विवरणात्मक व्याकरण – Hindi Grammer PDF Free Download
